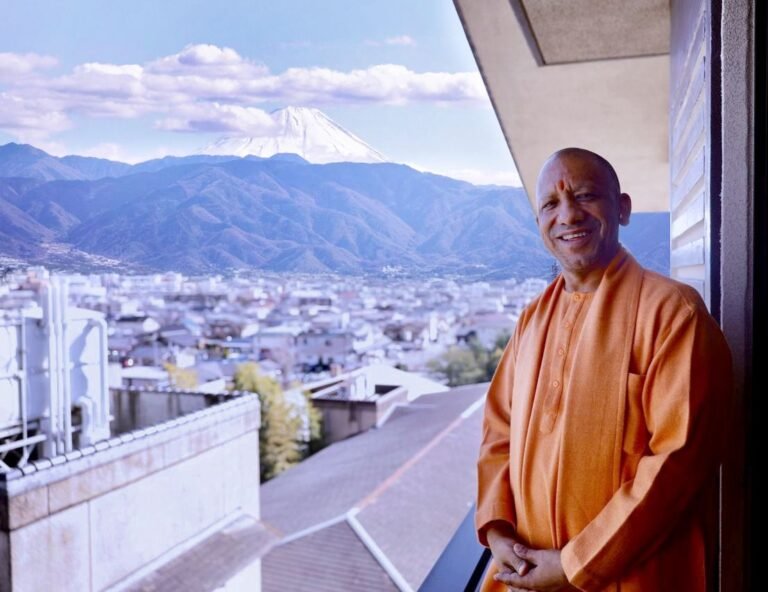संसद के शीत सत्र की अवधि केवल 15 दिन रखी गई है। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था को कितना सीमित समय दिया जा रहा है। संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले एक दशक में संसद के सत्र लगातार छोटे होते गए हैं- न तो मानसून सत्र अपनी औसत अवधि तक चलता है, न ही बजट सत्र। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब सरकार स्वयं को जनता-केन्द्रित और पारदर्शी बताती है।
सवाल है—आखिर सरकार संसद को लंबा क्यों नहीं चलाना चाहती?
जब विपक्ष SIR पर चर्चा की मांग करता है, तो प्रधानमंत्री इसे ड्रामा कह देते हैं। क्या लोकतंत्र में किसी भी विषय पर चर्चा की मांग करना ड्रामा है? SIR एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे नागरिकों की पहचान, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा है। अगर इसमें सब कुछ सही है, तो बहस से डर कैसा? और अगर खामियां हैं, तो उन्हें उजागर होना ही चाहिए।
लेकिन सरकार का रुख साफ दिख रहा है- कठिन सवालों से दूरी। संसद चलनी चाहिए, लेकिन नियंत्रित गति से; बहस होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ उन्हीं मुद्दों पर जिनका जवाब देना आसान हो।
विपक्ष की हर मांग को अस्वीकार कर देना अब सामान्य राजनीतिक शैली बन चुकी है। विशेष सत्र की मांग हो, जांच की मांग हो या किसी नीति पर बहस की, सरकार का पहला जवाब अक्सर यही होता है—अनावश्यक राजनीति। यह रवैया किसी पार्टी से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से मुकाबला करता है।
सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम का यह बयान कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, यह संकेत देता है कि सरकार किसी भी आलोचना को पहले से ही खारिज मानकर चल रही है। पर क्या विपक्ष को चुप कर देने से सवाल खत्म हो जाते हैं? नहीं। सवाल तो वहीं खड़े रहते हैं, सिर्फ़ उनका उत्तर देने का दायित्व टल जाता है- और यही चिंता की जड़ है।
दूसरी ओर, देश राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा में सांस ले रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई प्रदूषण का बोझ झेल रहा है। अस्पतालों में सांस और फेफड़ों की बीमारी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कई शहर WHO मानकों से 8–10 गुना अधिक प्रदूषित हैं।
ऐसे समय में प्रधानमंत्री का यह कहना कि दिल्ली का मौसम अच्छा लग रहा है- यह सिर्फ़ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस पूरे संकट की अनदेखी है जिसे जनता रोज़ झेल रही है। यह अनदेखी आने वाले समय में भारी पड़ेगी।
आज विपक्ष को ड्रामा कहा जा रहा है। कल जब जनता अपनी तकलीफों पर आवाज उठाएगी, तब उसे क्या कहा जाएगा? जब दस साल बाद कोई मरीज फेफड़ों के इलाज के लिए अपना घर बेच देगा, तब उसे शायद याद आएगा कि संसद में मुद्दों पर बहस हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। जब कोई पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश करेगा, तो उसे याद आएगा कि मुद्दों को हमेशा ड्रामा कहकर टाला गया।
और जब कोई सांसद फिर से जनता के सामने खड़ा होगा, तो उसे समझ आएगा कि 15 दिनों वाला सत्र लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम था।संसद किसी सरकार का नहीं, देश का संस्थान है। उसका छोटा होना सिर्फ़ विपक्ष को नहीं, हर नागरिक को कमजोर करता है। सरकार को यह समझना होगा कि वादों नहीं, बहसों से लोकतंत्र चलता है—और बहसों से ही भरोसा बनता है।