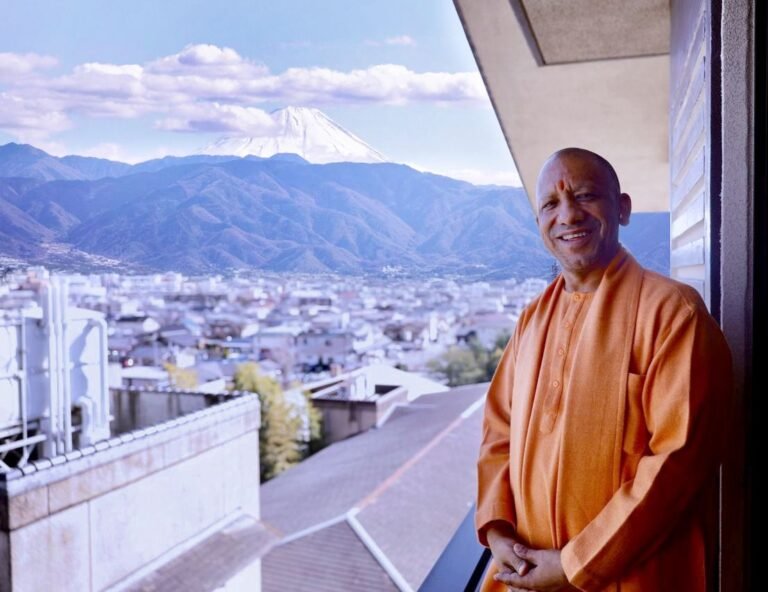बिहार में चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटने की योजना शुरू की। सवाल यह नहीं कि महिलाओं को आर्थिक मदद मिली—सवाल यह है कि यह मदद चुनाव से ठीक पहले और आचार संहिता लागू होने के बाद क्यों जारी रखी गई?
आचार संहिता 06 अक्टूबर को लागू हुई। इसके बाद भी सरकार ने चार बार पैसा बांटा—
17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, और 07 नवंबर।
यानी पूरे महीने सरकारी मशीनरी वोटरों के घर-घर पहुंचकर यह संदेश दे रही थी कि “सरकार याद कर रही है”—लेकिन चुनावी भाषा में इसे कहते हैं वोट पकड़ने का सीधा प्रयास।
सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उठता है। आयोग का काम लोकतंत्र की निष्पक्षता की रक्षा करना है, लेकिन इस बार वह धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे बैठा दिखा।
न तो रोक,
न कोई निर्देश,
न कोई कार्रवाई।
क्या आयोग को यह नहीं पता था कि चुनाव के बीच में पैसा बांटना चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है?
या फिर सत्ता पक्ष की सुविधा के लिए आंखें बंद कर ली गईं?
बीजेपी की रणनीति भी साफ दिखती है। बिहार में जमीन कमजोर है, तो चुनाव से पहले “लाभार्थी” राजनीति को तेज कर दिया गया। जनता के पैसे से जनता को ही साधने की यह नीति लोकतांत्रिक नहीं—बल्कि नैतिक गिरावट का उदाहरण है।
अगर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की योजनाएं चल सकती हैं और आयोग कुछ नहीं करेगा, तो फिर हर चुनाव में सत्ता पक्ष यही मॉडल अपनाएगा। यह लोकतंत्र नहीं—चुनावी प्रबंधन बन जाएगा।
बिहार की महिलाएं सशक्तिकरण की हकदार हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह नहीं होना चाहिए।और चुनाव आयोग को याद रखना चाहिए—चुप्पी भी कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है।